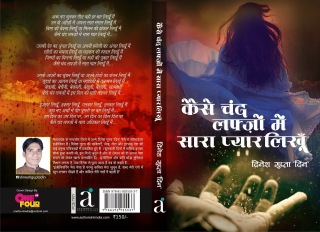एक शहर है, बहुत विशाल, लोगों से भरा, लोगों से डरा, मकानों से पटा, सटा-सटा। ये शहर
‘बड़ा शहर’ है। एक है इसका उलट, छोटा सा, आधे घंटे में एक छोर से उस छोर, कम लोग, नीचे मकान, खाली सड़कें, बिलकुल विपरीत,
‘छोटा शहर’।
 |
| मस्त, अपना शहर vs व्यस्त बड़ा शहर (चित्र साभार गूगल) |
अभी मैं बड़े शहर का बाशिंदा हूँ, या यूँ कहें कि यहाँ एक मुसाफिर हूँ। हाँ मुसाफिर ही कहूँगा। यह एक बस स्टॉप की तरह है। भीड़-भाड़, गन्दगी, दहशत, संदेहास्पद मुसाफ़िर और लोगों का आना जाना। यहाँ पर शहर का लोगों पर ज़ोर है। उसी के हिसाब से लोग चलते हैं। लोगों को शहर का खौफ़ है। वो शहर जो खुद तो अदृश्य है पर लोगों पर हुकूमत चलाता है, भगवान की तरह?
मेरे जैसे मुसाफ़िर जो छोटे शहरों को अपना दिल बेच चुके हैं, उनको यह बस स्टॉप कभी पसंद नहीं आ सकता। यहाँ लोग दौड़ते-भागते रहते हैं, मुझे तो लोगों को ठहरे हुए देखने की आदत है, उनके चहरे को पढ़ने की आदत, उनके भावों को समझने की आदत, उनसे बतियाने की आदत, उनके साथ चाय पीने की आदत। ये आदत बड़े शहरों में ख़राब हो गई है। कोई रुकता ही नहीं है जिसको मैं समझ सकूं, जो मुझे समझ सके। कोई रुकता नहीं है ५ मिनट के लिए जिससे दोस्ती कर सकूँ, जिसके साथ चाय पी सकूँ। यहाँ लोग चाय कॉफ़ी पर तभी मिलते हैं जब उन्हें कोई काम निकलवाना होता है। छोटे शहरों में जब कोई काम नहीं होता तो चाय पर मिल जाते हैं, अक्सर हर शाम।
बड़े शहरों में ऊँची ऊँची दीवारें है। घरों और दिलों, दोनों के बीच। न तुम मुझे जानते हो, न मैं तुम्हें। “क्या तुम मेरे पड़ोस में पिछले १ साल से रह रहे हो? कभी गौर नहीं किया।” ये आम वाक्य है लोगों के। छोटे अपने शहर में कोई एक दिन के लिए भी अनजान नहीं रहता। मैं अपने मोहल्ले में सबको नाम से जानता हूँ, पहचानता हूँ। वहाँ अभी भी पैसों के लिए अनजान नहीं होते हैं। अभी कुछ समय पहले बड़े शहर में मेरे नीचे तल्ले के बाशिंदे की तबियत ख़राब हुई थी। मुझे पूरे एक हफ्ते बाद दरबान से पता चला कि वो अस्पताल में भरती हैं। अब जा कर मिलने में भी संकोच हो रहा है। कुछ चीज़ें समय निकलने के बाद करनी मुश्किल हो जाती हैं। अपने शहर में छींक आने पर भी ५ लोग पूछ लेते हैं कि क्या दवा-पानी चल रहा है और नसीहत इतनी दे जाते हैं कि बिमारी से ज़्यादा नसीहतों का डर लगने लगता है। बड़े शहर के कई मुसाफिर कहते हैं कि “यहाँ ठीक है, कोई परेशान नहीं करता अपनी नसीहतों से।” पर सच तो यह भी है कि आदमी को मरे हुए ३ दिन निकल जाते हैं और दुर्गन्ध से ही पता चलता है कि वो तो गया। ३ दिन के अंतर और नसीहतों के समंदर के बीच फैसला ऐसी घटनाओं से ही हो जाता है।
मैंने कभी अपने शहर में लोगों को हर दिन ऐसे भागते हुए नहीं देखा कि मानों पागल कुत्ता पीछे पड़ा हो। वैसे कभी-कभार कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं तो भागना पड़ता है। बड़े शहरों में मैंने मुसाफिरों को हर दिन केवल भागते ही तो देखा है। बसों में, ट्रेनों में, ट्रकों में, मेट्रो में, गाड़ियों में, बाईकों में, सब तरफ लोगों के बीच एक ऐसी अनकही-अदृश्य दौड़ है जिसका अंत किसी को नहीं पता और न ही इस दौड़ का कोई विश्लेषण कर पाया है। मेट्रो के दरवाज़ों के खुलते ही लोग बैलून में से हवा निकलने की प्रक्रिया को हुबहू नक़ल करते हैं। ऐसा लगता है कि वो निर्जीव मेट्रो भी अब इनके निकलने पर सांस ले पा रहा है। हर तरफ अफरा-तफरी मची हुई है। कोई किससे भिड़ रहा है, कोई किससे लड़ रहा है। किसी के केश अगर किसी के हाथों को छू जाए तो लात-घूँसे चल जाते हैं। ये मुसाफिर वही लोग हैं जो छोटे शहरों से हैं। क्योंकि उन्होंने कभी इतनी भीड़ को झेला नहीं होता है तो यहाँ आ कर बौरा जाते हैं। अपने शहर में मैं केवल परिचितों से भिड़ता हूँ, यदा-कदा बाज़ार में। कभी किसी अनजान से भिड़ गया तो भी एक हँसी से बात आई-गई हो जाती है।
बड़े शहरों में लोग कमाने आते हैं पर खुद को बेच देते हैं। अपना शरीर, अपना ज़मीर। कईयों को तो इसके लिए मुँह-माँगे दाम भी नहीं मिलते हैं। अपने शहर में लोग इतनी आसानी से बिकाऊ नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ समाज की पकड़ मज़बूत है, उसका डर है, उसकी नज़र है। बड़े शहर में समाज को तड़ीपार कर दिया गया है। यहाँ समाज बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ दीवारें बहुत ऊँची हैं और ऊँची दीवारों से तो आजतक बँटवारा ही हुआ है। नहीं?
बड़े शहर के लोग हर दिन चीखते चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं पर दिक्कत ये है कि हर कोई अपनी शोर मचा रहा है। कोई सुनने वाला ही नहीं है। यही कारण है कि लोग दुखी हैं। उनके दुःख को वो किसे सुनाएँ? मेरे शहर में चीखने चिल्लाने की नौबत नहीं आती। संतुष्ट लोगों को सुनने की आदत ज्यादा होती है। किसी एक को सुनने के लिए हजारों कान हैं। यहाँ संतुष्टि है तो शान्ति है। वहाँ शोर है तो अशांति है।
मैं तो यहाँ सिर्फ मुसाफ़िर ही बन कर रहना चाहता हूँ। मैं कभी इस बड़े शहर को ‘अपना’ शहर नहीं कह पाऊँगा। अगर यहाँ जन्मता-बढ़ता तो शायद ऐसा हो पाता। मुझे अपने शहर पहुँचना है। वहाँ से निकला तो हूँ पर वहीँ वापस पहुँचने के लिए। कैसी अजीब विडम्बना है ये ज़िन्दगी।
वैसे एक सच तो यह भी है कि शहर किसी का नहीं होता। न मेरा न तुम्हारा। वह तो मूक दर्शक की भांति सबको देखता-तकता रहता है और मंद-मंद मुस्कुराता रहता है कि कैसे बेवकूफ है यहाँ के लोग जो उसे अपना कहते हैं जबकि वह उनके रुदन पर कभी नहीं रोता है, उनकी ख़ुशी में कभी नहीं हँसता है। पर एक सत्य यह भी है कि ज़िन्दगी को पार करने के लिए एक ऐसा सहारा चाहिए जो बस इस सफ़र तक हमारा हो। एक शहर को अपना कहकर आदमी के दिल को ठंडक मिल जाती है और उसका सफ़र थोड़ा कम कष्टदायक हो जाता है।
चलिए निकलता हूँ एक रिश्तेदार से मिलने। आज का पूरा दिन इसी मिलने के नाम है। अपने शहर में तो हम अपने सभी रिश्तेदारों से दिन में दो बार मिल आते हैं। ये बड़ा शहर मुझे कभी रास नहीं आया।